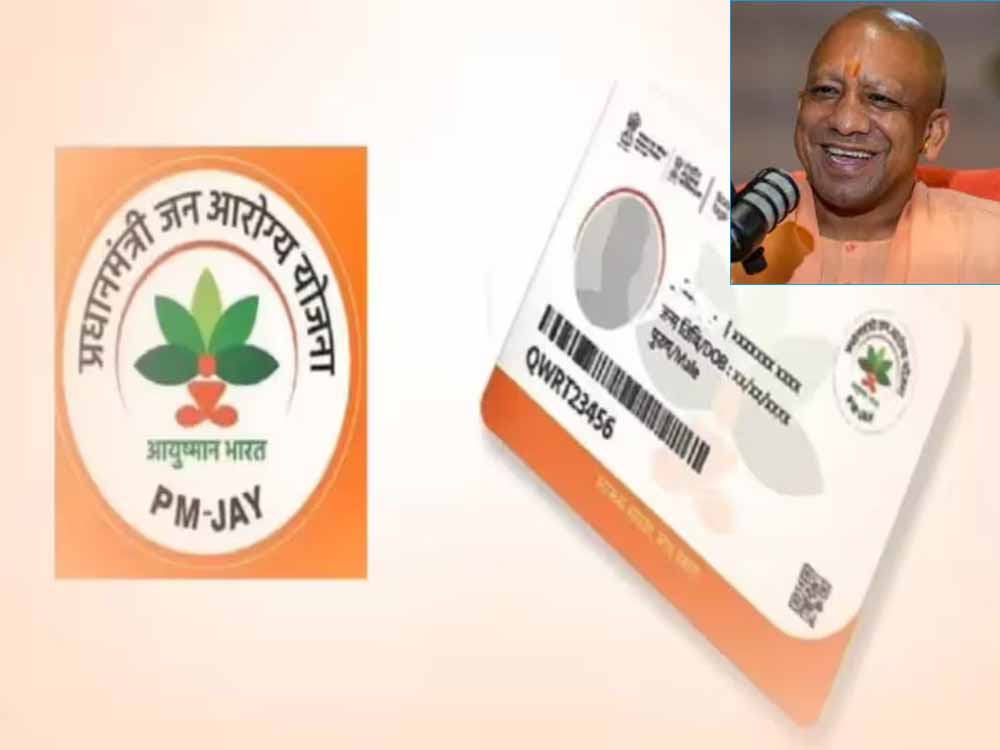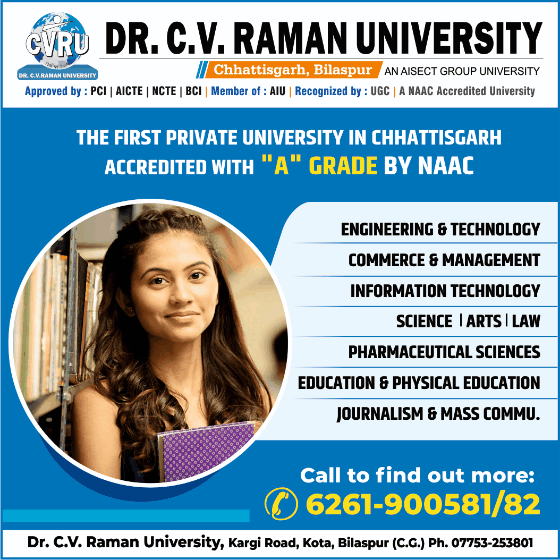नई दिल्ली
देश के शहरी परिवहन में तेजी लाने और स्थायी परिवहन समाधान सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कई परिवर्तनकारी पहल शुरू की हैं। इन कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेट्रो परियोजनाएं टिकाऊ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से उन्नत हों। दूरदर्शी नीतियों, साहसिक निवेशों और स्मार्ट साझेदारियों के माध्यम से, सरकार एक स्वच्छ, तेज़ और अधिक कनेक्टेड शहरी भविष्य की नींव रख रही है।
भारत का मेट्रो नेटवर्क 248 किमी (2014) से बढ़कर 1,013 किमी (2025) हो गया है। भारत ने ₹2.5 लाख करोड़ (28.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया है और घरेलू स्तर पर 2,000 से ज्यादा मेट्रो कोच बनाए हैं। वहीं, मेक इन इंडिया, सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेशन और चालक रहित मेट्रो जैसी पहल स्वच्छ और भविष्य के लिए तैयार परिवहन (मोबिलिटी) को बढ़ावा दे रही हैं।
भारत की मेट्रो यात्रा इसकी शहरी जागृति का प्रतीक
वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में दिल्ली के बड़े उपनगरों में बिछाई गई पहली रेल पटरियों से लेकर अब 20 से ज्यादा भारतीय शहरों में फैले व्यस्त, तकनीक-संचालित नेटवर्क तक, भारत की मेट्रो यात्रा इसकी शहरी जागृति का प्रतीक है। तेज जन परिवहन की दिशा में एक सतर्क कदम के रूप में शुरू हुआ यह सफर आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया है, जिसने दैनिक आवागमन को सुव्यवस्थित किया है, शहर की भीड़भाड़ को कम किया है और इस क्षेत्र को नया आकार दिया है।
देखा जाये तो, मेट्रो अब केवल परिवहन का एक साधन नहीं है, यह भारत की विकास गाथा के केंद्र में धड़कती एक जीवनरेखा है, जो महत्वाकांक्षा, नवाचार और टिकाऊ शहरी जीवन के दृष्टिकोण से प्रेरित है। भारत अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के रूप में गर्व से खड़ा है, जिससे शहरी परिवहन विस्तार में इसकी तेज प्रगति का पता चलता है।
परिचालन का विस्तार
आपको बता दें, भारत का परिचालन मेट्रो नेटवर्क 5 शहरों में 248 किमी (2014) से बढ़कर मई 2025 तक 23 शहरों में 1,013 किमी हो गया है, यानी केवल 11 वर्षों में 763 किमी की वृद्धि हुई है। औसत दैनिक सवारियों की संख्या 28 लाख (2013-14) से बढ़कर 1.12 करोड़ से अधिक हो गई है, जो शहरी आवागमन में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है।
मेट्रो विकास के आंकड़े
नई लाइनें चालू करने की गति नौ गुना बढ़ गई है: 0.68 किमी/माह (2014 से पहले) से बढ़कर आज लगभग 6 किमी/माह हो गई है।
2025-26 के लिए वार्षिक मेट्रो बजट ₹34,807 करोड़ है, जो 2013-14 के ₹5,798 करोड़ से छह गुना से भी अधिक है।
भविष्य की दिशा: सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम-
मेट्रो रेल नीति, 2017
मेट्रो रेल नीति 2017 शहरों को कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान्स (सीएमपी) तैयार करने और शहरी महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) स्थापित करने का निर्देश देती है ताकि मेट्रो प्रणालियों के विकास का मार्गदर्शन किया जा सके और स्थिरता, आर्थिक व्यवहार्यता और एकीकृत शहरी गतिशीलता पर विशेष बल दिया जा सके। केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, मेट्रो परियोजनाओं को न्यूनतम 14% का इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (ईआईआरआर) सुनिश्चित करना होगा और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निजी क्षेत्र की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
मेट्रो रेल प्रणालियों के लिए मेक इन इंडिया
महत्वाकांक्षी मेक-इन-इंडिया अभियान के तहत, सरकार ने कम से कम 75% मेट्रो कारों और 25% प्रमुख उपकरणों व उप-प्रणालियों की घरेलू खरीद का प्रावधान किया है- यह स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक साहसिक कदम है।
वहीं, पिछले दस वर्षों में, भारत ने अपने मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में लगभग ₹2.5 लाख करोड़ (28.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया है। इस गति ने मेट्रो कोचों के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा दिया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) ने मई 2024 तक दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में 2,000 से अधिक मेट्रो कोचों की आपूर्ति की है, जिससे घरेलू क्षमताएं मज़बूत हुई हैं और आयात पर निर्भरता कम हुई है।
वैश्विक साझेदारियों से मेट्रो नेटवर्क के विकास को भी गति
वैश्विक साझेदारियां देश में मेट्रो नेटवर्क के विकास को भी गति दे रही हैं। ऐसी ही एक परियोजना, मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एमएमएल-3), ₹23,136 करोड़ (2.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के भारी निवेश से शहरी परिवहन में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगी। ₹13,235 करोड़ (1.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या कुल वित्तपोषण का 57.2%, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा ऋण सहायता के रूप में प्रदान किया जा रहा है। शेष धनराशि भारत सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार/मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जा रही है, जो इसे बुनियादी ढांचे के विकास में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सहयोग का एक सशक्त उदाहरण बनाता है।
ग्रीन अर्बन मोबिलिटी
भारत की मेट्रो रेल प्रणालियां हरित नवाचारों को अपना रही हैं। दिल्ली मेट्रो ने ओखला विहार में एक एलिवेटेड वायडक्ट पर एक वर्टिकल बाइ-फेसियल सोलर प्लांट और खैबर पास डिपो में 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया है, जो भूमि-मुक्त नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जैसी अन्य हरित पहल, जिन्हें महानगरों में व्यापक रूप से अपनाया गया है, ब्रेकिंग ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करके बिजली बचाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली, कोच्चि, नागपुर और पुणे जैसे शहरों के कई मेट्रो स्टेशनों को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) प्रमाणन प्राप्त हुए हैं, जो पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हैं। ये प्रयास भारत के स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप हैं और स्वच्छ शहरी गतिशीलता में मेट्रो की बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं।
भारत की मेट्रो रेल में अत्याधुनिक नवाचार
उल्लेखनीय है, देश की मेट्रो प्रणालियां न केवल आकार में बढ़ रही हैं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता भी विकसित हो रही है। स्वचालन, डिजिटलीकरण और स्थिरता की ओर बढ़ते ज़ोर के साथ, देश भर की मेट्रो कंपनियां नई तकनीकों को अपना रही हैं।
नमो भारत ट्रेन
भारत की पहली अत्याधुनिक हाई-स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन
160 किमी/घंटा की परिचालन गति (डिजाइन गति: 180 किमी/घंटा) पर चलती है।
दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) पर चलाई गई
अंडरवाटर मेट्रो
2024 में, भारत ने कोलकाता में अपनी पहली अंडरवाटर मेट्रो सुरंग शुरू करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो हुगली नदी के नीचे एस्प्लेनेड को हावड़ा मैदान से जोड़ेगी।
इंजीनियरिंग का यह चमत्कार भारत की बढ़ती तकनीकी और अवसंरचनात्मक क्षमता का प्रतीक है।
वाटर मेट्रो
केरल का कोच्चि, वाटर मेट्रो शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया।
वाटर मेट्रो निर्बाध और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड नावों का उपयोग करके 10 द्वीपों को जोड़ती है
यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ईटीसीएस) लेवल II सिग्नलिंग
एलटीई रेडियो बैकबोन का उपयोग करते हुए हाइब्रिड लेवल III सिस्टम वाला दुनिया का पहला ईटीसीएस लेवल II।
नमो भारत मार्ग पर ट्रेन सुरक्षा, गति और वास्तविक समय की निगरानी को बेहतर बनाता है।
प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (पीएसडी)
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित।
यात्री सुरक्षा को बढ़ाता है और प्लेटफॉर्म-स्तरीय दुर्घटनाओं को कम करता है।
नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
एकीकृत एक राष्ट्र, एक कार्ड समाधान।
मेट्रो, बसों, उपनगरीय रेल, टोल और खुदरा दुकानों में निर्बाध यात्रा को सक्षम बनाता है।
क्यूआर-आधारित टिकटिंग
मोबाइल ऐप-आधारित क्यूआर टिकट, टिकटिंग अनुभव को सरल और डिजिटल बनाते हैं।
मानवरहित रेल संचालन (यूटीओ)
गौरतलब हो, दिल्ली मेट्रो के कई हिस्सों में चालक रहित तकनीक काम कर रही है, और इसकी शुरुआत 2020 में मैजेंटा लाइन पर की गई थी। इससे दक्षता बढ़ती है और मानव निर्भरता कम होती है।
स्वदेशी स्वचालित रेल पर्यवेक्षण प्रणाली (आई-एटीएस)
भारत में पहली बार स्थानीय स्तर पर विकसित, एटीएस रेल संचालन और सिग्नलिंग का स्वचालित स्थानीय और केंद्रीय नियंत्रण और निगरानी प्रदान करता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और बीईएल द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित, यह प्रणाली अब दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर सक्रिय है।
प्रस्तावित मेट्रो परियोजनाएं
भारत में मेट्रो का विस्तार योजना और अनुमोदन के चरणों में नई परियोजनाओं की बाढ़ के साथ गति पकड़ रहा है। इसका उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार, शहरी विकास को बढ़ावा देना और उभरते और स्थापित शहरों में स्वच्छ, तेज और अधिक समावेशी सार्वजनिक परिवहन प्रदान करना है। इन आगामी परियोजनाओं में से कुछ इस प्रकार हैं-
पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण-2
पुणे मेट्रो चरण-2, जिसमें 13 स्टेशनों के साथ 12.75 किमी लंबाई का दो एलिवेटेड कॉरिडोर (वनाज़-चांदनी चौक और रामवाड़ी-वाघोली) शामिल है, को मंजूरी दे दी गई है और इसे चार वर्षों के भीतर पूरा करने की योजना है। विस्तार से आईटी केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और इंटरसिटी बस टर्मिनलों तक पहुंच में सुधार होगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बढ़ेगा।
दिल्ली मेट्रो
एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर का इंदिरा गांधी घरेलू टर्मिनल-1 तक विस्तार (2.16 किमी, भूमिगत)।
मैजेंटा लाइन विस्तार (लाइन 8) – रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (9.913 किमी, भूमिगत)।
गोल्डन लाइन विस्तार (लाइन 10) – तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज (9 किमी, एलिवेटेड)।
नोएडा सेक्टर-51 से नॉलेज पार्क V (17.435 किमी)।
अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण-2ए
सरदार वल्लभभाई पटेल हवाई अड्डे (6.032 किमी) से सीधी कनेक्टिविटी के लिए अहमदाबाद मेट्रो का विस्तार।
इस विस्तार से दैनिक यात्रियों, हवाई अड्डे के कर्मचारियों और शहर भर के निवासियों के लिए हवाई अड्डे तक सुविधाजनक और तेज पहुंच सुनिश्चित होगी।
बेंगलुरु मेट्रो चरण-3
केंद्र सरकार ने ₹15,600 करोड़ की लागत से चरण-3 के 45 किमी हिस्से को मंजूरी दी है।
वर्तमान में, शहर में 75 किमी मेट्रो चालू है और 145 किमी निर्माणाधीन है।
जल मेट्रो का विस्तार
कोच्चि मेट्रो के मॉडल के अनुरूप, सरकार ने असम के गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर सहित भारत भर के 24 शहरों में जल मेट्रो विस्तार सेवाओं के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार से कनेक्टिविटी में सुधार, सड़क भीड़भाड़ को कम करने और शहरों में स्थायी परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
दरअसल, दिल्ली के चहल-पहल वाले प्लेटफॉर्म से लेकर सूरत और भोपाल की उभरती हुई रेल लाइनों तक, मेट्रो चुपचाप एक नए भारत का ताना-बाना बुन रही हैं, जो तेज, कुशल और स्वच्छ हैं। ये सिर्फ़ ट्रेनें नहीं हैं, ये कल के भारत की जीवनरेखा हैं, जो न सिर्फ यात्रियों को, बल्कि महत्वाकांक्षा, समानता और लचीलापन भी प्रदान करती हैं।
भारत 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है, ऐसे में मेट्रो रेल जैसा मजबूत सार्वजनिक परिवहन इसके विकास की रीढ़ बनेगा, लोगों को जोड़ेगा, शहरों को ऊर्जा प्रदान करेगा और पृथ्वी की रक्षा करेगा।